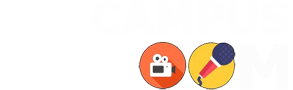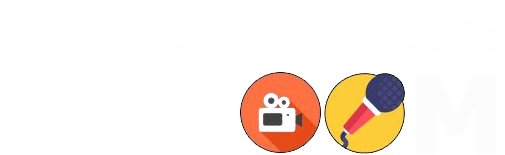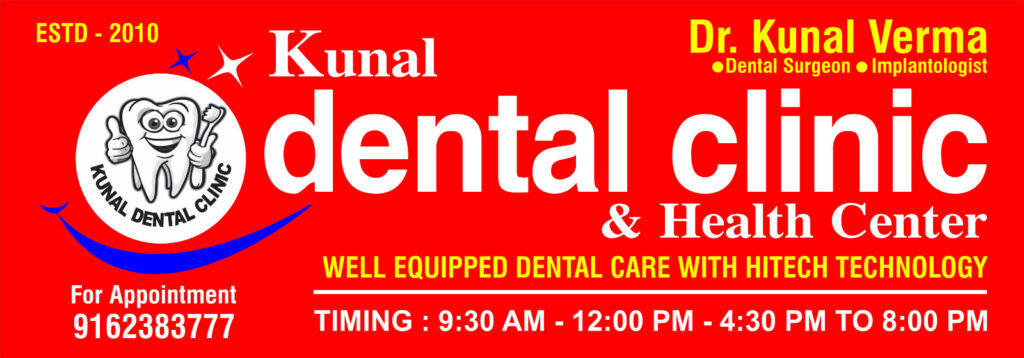– स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य के लिए मातृ स्वास्थ्य पर टाटा मेन हॉस्पिटल की डॉ अलोकानंदा रे की पढ़े ये विशेष रिपोर्ट
इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय – स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य – एक मजबूत संकल्प के साथ सामने आया है: मातृ और नवजात स्वास्थ्य को इस स्तर तक पहुंचाना जहां कोई भी बीमारी या मृत्यु, जिसे रोका जा सकता है, वह न हो। यह न सिर्फ एक संदेश है, बल्कि एक वैश्विक आह्वान है कि सभी स्वास्थ्य संस्थाएं, सरकारें और समाज मिलकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें, जहां माताओं और नवजातों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इस अवसर पर हमें यह सुनिश्चित करना है कि न केवल सेवाओं की गुणवत्ता बढ़े, बल्कि उनका बुनियादी ढांचा मजबूत हो और सबसे अहम – हर वर्ग, हर क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों तक ये सेवाएं समान रूप से पहुंचें। तभी हम वास्तव में एक स्वस्थ और आशावादी भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।
पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इन पहलों की बदौलत भारत की मातृ मृत्यु दर (MMR) में निरंतर गिरावट आई है, जो अब 1,00,000 जीवित जन्मों पर 97 तक पहुँच चुकी है। उल्लेखनीय है कि देश के कुछ राज्य पहले ही 70 से कम मातृ मृत्यु दर हासिल कर चुके हैं—जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 2030 तक निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) का मानक है।
हालांकि, इस सफर को और सशक्त बनाने के लिए हमें गर्भावस्था से पहले की तैयारी को प्राथमिकता देनी होगी। सफल और सुरक्षित प्रसव की कुंजी है गर्भ से पूर्व परामर्श और देखभाल। इसका मतलब है कि गर्भावस्था योजनाबद्ध होनी चाहिए—जहां महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का मूल्यांकन पहले ही कर लिया जाए और कुपोषण, एनीमिया जैसी पहले से मौजूद बीमारियों का प्रभावी इलाज गर्भधारण से पहले सुनिश्चित किया जाए। यही सोच हमें सुरक्षित मातृत्व और एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में ले जाएगी।
गर्भावस्था के दौरान, मां को समय-समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) अवश्य करानी चाहिए, जिसमें आवश्यक चिकित्सकीय जांच और परीक्षण शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया गर्भधारण के पहले तीन महीनों के भीतर शुरू हो जानी चाहिए और पूरी गर्भावधि में नियमित रूप से जारी रहनी चाहिए।
इस दौरान पोषण का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती महिला का आहार संतुलित होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त कैलोरी के साथ उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व—जैसे विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स—शामिल हों। साथ ही, नियमित व्यायाम और मादक पदार्थों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। इन पहलुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि यही स्वस्थ गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव की बुनियाद हैं।
एलबीएसएम कॉलेज में होगा दो दिवसीय अंर्तराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन
हर गर्भावस्था की सफल और सुरक्षित देखभाल में पोषण सप्लीमेंटेशन और टीकाकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की नियमित खुराक न केवल मां के शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि भ्रूण के स्वस्थ विकास की नींव भी रखती है। ये सप्लीमेंट्स रक्ताल्पता, हड्डियों की कमजोरी और जन्म दोष जैसे जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसी तरह, टिटनेस, डिप्थीरिया, फ्लू और काली खांसी (व्हूपिंग कफ) जैसे संक्रमणों के खिलाफ समय पर दिया गया टीकाकरण मां और नवजात दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये टीके गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के खतरे को कम करते हैं और शिशु को जन्म के बाद शुरुआती महीनों में गंभीर बीमारियों से बचाते हैं।
स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों के साथ नियमित प्रसवपूर्व जांच (ANC) गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं की समय रहते पहचान करने में बेहद सहायक होती है। उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन मधुमेह, पीलिया और अन्य चिकित्सकीय या प्रसूति संबंधी समस्याएं अगर समय पर पहचान ली जाएं और उनका तुरंत इलाज शुरू हो जाए, तो कई तरह की जटिलताओं और जोखिमों से बचा जा सकता है। इस तरह की नियमित निगरानी मां और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।
सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल, मातृत्व की ओर बढ़ती गर्भावस्था की इस सुंदर यात्रा की पूर्णता को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में भारत में संस्थागत प्रसव की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रसव के दौरान और उसके बाद चिकित्सा देखरेख सुनिश्चित की जा रही है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है, जो मातृ और नवजात स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पहुंच दोनों में सुधार को दर्शाता है।
विशेष रूप से जटिल या उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के मामलों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से द्वितीयक या तृतीयक देखभाल केंद्रों तक प्रभावी रेफरल सिस्टम की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल गंभीर जटिलताओं से समय पर निपटने में मदद करता है, बल्कि मातृ मृत्यु दर और बीमारियों को भी काफी हद तक कम करता है।
प्रसव के बाद मां और शिशु दोनों की समग्र देखभाल का एक नया चरण शुरू होता है, जो इस पूरी यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। इस चरण में स्वास्थ्य विशेषज्ञों से नियमित परामर्श जारी रखना बेहद ज़रूरी है। नवजात की देखभाल, स्तनपान की सही तकनीक, मां के पोषण का ध्यान, आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन, तथा गर्भावस्था के दौरान बढ़े वजन को कम करने के लिए उचित व्यायाम—ये सभी पहलू मां के स्वास्थ्य को फिर से संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले तत्काल प्रभावों से आगे बढ़ते हुए, हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि गर्भ में शिशु का विकास एक अत्यंत निर्णायक चरण होता है—जो न केवल बचपन, बल्कि पूरे जीवनकाल में होने वाली बीमारियों की जड़ों से जुड़ा होता है।
जब भ्रूण के अंगों का निर्माण हो रहा होता है, तब मां के गर्भ का वातावरण—यदि तनावपूर्ण या असंतुलित हो (जैसे कुपोषण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य चिकित्सा स्थितियां)—तो यह भ्रूण की आनुवंशिक संरचना के साथ मिलकर बच्चे के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। यह परिस्थिति आगे चलकर मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और मानसिक विकार जैसी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकती है।
गर्भ के भीतर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भ्रूण कई बार स्वयं को अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में कुछ जींस में स्थायी परिवर्तन हो सकते हैं, जो आगे चलकर जीवन के विभिन्न चरणों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इन बीमारियों में त्वचा संबंधी एलर्जी, अस्थमा, एक्ज़िमा, संक्रमण के प्रति बढ़ी संवेदनशीलता, मोटापा, मधुमेह, मानसिक व न्यूरोलॉजिकल विकार, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर (विशेषकर रक्त, यकृत और वृषण कैंसर) शामिल हो सकते हैं।
इसे ‘फीटल प्रोग्रामिंग’ कहा जाता है—एक ऐसा सिद्धांत जो यह संकेत देता है कि मां में पोषण असंतुलन (चाहे कमी हो या अधिकता), साथ ही चयापचय संबंधी गड़बड़ियां, विशेष रूप से गर्भकालीन मधुमेह, भ्रूण के स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकती हैं। इसका असर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है, जिससे न केवल बचपन में, बल्कि आगे चलकर वयस्क जीवन में भी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य न केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा भी है। इसका प्रभाव केवल सुरक्षित प्रसव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दीर्घकालिक रूप से समाज की स्वास्थ्य संरचना को भी प्रभावित करता है। आज जब मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियां वैश्विक महामारी बन चुकी हैं, तब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन रोगों की जड़ें अक्सर गर्भकाल के दौरान ही पड़ जाती हैं।